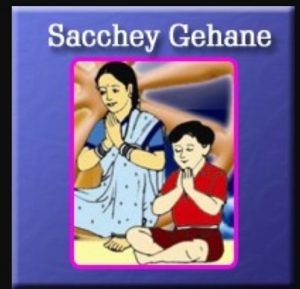
हिम शिखर ब्यूरो
१९वीं शताब्दी का यह प्रसंग है। बंगाल के मेदिनापुर जिले के वीरसिंह गाँव के एक बालक ने अपनी माँ से कहा: ‘‘माँ! मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊँ।”
माँ बोली: ‘‘हाँ बेटा! बहुत दिनों से मुझे तीन गहनों की चाह है।”
उत्सुकतापूर्वक बालक ने पूछा: ‘‘माँ! कौन-से तीन गहने?”
‘‘बेटा! इस गाँव में कोई विद्यालय नहीं है, इसलिए मेरी पहली चाह यह है कि यहाँ एक अच्छा विद्यालय हो। दूसरा, गाँववालों की चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं है, मैं चाहती हूँ यहाँ एक दवाखाना खुले। तीसरा, गरीब और अनाथ बच्चों में भोजन व खाद्य-सामग्री बाँटी जाय। बस, यही वे तीन गहने हैं जिनकी मुझे चाह है।”
माँ की बातें सुनकर बालक की आँखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठीं, हृदय परोपकार की भावना से भर गया और सिर माँ के चरणों में झुक गया। उसने माँ के कहे अनुसार तीनों गहने बनवा दिये। वीरसिंह गाँव का ‘भगवती विद्यालय’ आज भी इसका साक्षी है। वह माँ थी भगवती देवी और बालक था ईश्वरचन्द्र, जो आगे चलकर पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। माँ के इन्हीं संस्कारों ने बालक ईश्वरचन्द्र में मानवीय संवेदनाओं का विकास किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरजी ने अपने जीवन में शिक्षा (विशेषकर स्त्री-शिक्षा) के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये, साथ ही चिकित्सा-सेवा, दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सेवा एवं नशामुक्ति हेतु भी कार्य किये। उन्होंने बंगाल में कई विद्यालय खोले। किसानों व मजदूरों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोलीं।
सन् १८७६ के बंगाल के भीषण अकाल में भूख से तड़पते लोगों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने सरकार के समक्ष अकाल पीड़ितों की दयनीय अवस्था का मार्मिक वर्णन कर सरकार द्वारा अन्नक्षेत्र खुलवाये, साथ ही स्वयं भी कई अन्नक्षेत्र खोले। किसीके बीमार होने की खबर मिलने पर वे स्वयं उसके पास जाते व दवा देकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करते। मानवेतर प्राणियों का वे कितना ख्याल रखते थे – इस बात को उजागर करनेवाला उनके जीवन का एक प्रसंग है।
 एक बार विद्यासागरजी से खुदीराम बोस मिलने आये। विद्यासागरजी ने खाने के लिए उन्हें नारंगियाँ दीं। वे नारंगियों को छीलकर उनकी फाँकें चूस-चूसकर फेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागरजी बोले :‘‘भाई! इन्हें फेंकिये मत। ये भी किसीके काम आ जायेंगी।”
एक बार विद्यासागरजी से खुदीराम बोस मिलने आये। विद्यासागरजी ने खाने के लिए उन्हें नारंगियाँ दीं। वे नारंगियों को छीलकर उनकी फाँकें चूस-चूसकर फेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागरजी बोले :‘‘भाई! इन्हें फेंकिये मत। ये भी किसीके काम आ जायेंगी।”
खुदीरामजी ने बड़े ही आश्चर्य के साथ विद्यासागरजी की ओर देखते हुए कहा : ‘‘आप इन्हें किसे देनेवाले हैं?” “विद्यासागरजी ने हँसकर उत्तर दिया: ‘‘आप इन्हें खिड़की के बाहर रख दीजिये और वहाँ से हट जाइये तो अभी पता चल जायेगा।” “चूसी हुई उन फाँकों को खिड़की के बाहर रखने पर कुछ कौवे उन्हें लेने के लिए आ गये। विद्यासागरजी ने कहा: ‘‘देखो भाई! जब तक कोई पदार्थ किसी भी प्राणी के काम में आने के योग्य हो, तब तक उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। उसे इस प्रकार रखना चाहिए कि धूल-मिट्टी लगकर वह नष्ट न हो जाय और दूसरे प्राणी उसका उपयोग कर सकें।”
उनकी परोपकारिता के बारे में सुनकर एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस उनसे मिलने आये। परमहंसजी ने कुशलक्षेम जानने के बाद कहा: ‘‘मैं अनेक दलदलों को पार करता हुआ अंत में अथाह सागर के किनारे आ पहुँचा हूँ और वह अब मेरे सामने है। आप ही वह विशाल महासागर हैं और मैं आपके भीतर से कुछ अमूल्य मोती चुनने आया हूँ। आशा है, मुझे खाली हाथों नहीं लौटना पड़ेगा ।”
विद्यासागरजी ने परमहंसजी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया: ‘‘आपने यहाँ पधारकर सचमुच मुझे कृतार्थ किया है लेकिन जिस सागर की खोज आप कर रहे हैं और जिसके पास आप आये हैं, वह सच्चा सागर नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसमें आपको कोई मोती नहीं मिलेगा। हाँ, मुट्ठीभर कौड़ियाँ अवश्य मिल सकती हैं। आपको उनसे ही संतोष करके लौटना होगा।”
वास्तव में सदगुणों के सागर होते हुए भी कितनी निरभिमानिता थी विद्यासागरजी में! परोपकार की चाह ही जिस माँ के गहने थे और निरभिमानता से अलंकृत निःस्वार्थ सेवा ही जिस पुत्र के जीवन का उद्देश्य था, वे सत्संगी माँ भगवती देवी व विद्यासागरजी धन्य हैं! ‘सबमें एक, एक में सब’ के सत्संग को पचाने वाली वह माता धन्य है!