
हिमशिखर धर्म डेस्क
अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह कौन है तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश व व्यवसाय का परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो, ऐसी बात नहीं। वस्तुत: उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को शरीर ही समझने लगा है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, परंतु अज्ञानतावश मानव अपने आपको शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ व अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं व व्यथाओं का घर बन जाता है।

मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर से दुर्गध होने लगती है। देह वही है, ज्यों की त्यों है, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट होता है कि मानव शरीर में निवास तो करता है पर वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं।
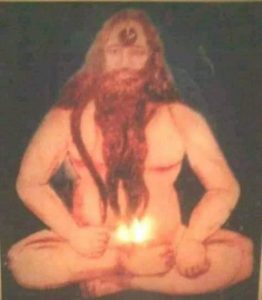
शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम-लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांतत: हम सब उसे मानते भी हैं। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्व साधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में अधिकतर लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों का व्यवहार ऐसा होता है मानो वे शरीर ही हैं।
किसी व्यक्ति का अगर सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है तब पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है।
शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वच्छता, स्वास्थ्य व सुविधा के लिए काम करना उचित और आवश्यक है, परंतु यह बात अहितकर है कि उसे केवल शरीर ही मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आपको शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि-लाभों को भी वह अपना हानि-लाभ मान लेता है और वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल-भूलैया का खेल जीवन को नीरस बना देता है।