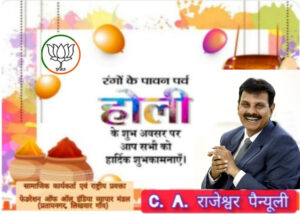हिंदू धर्मशास्त्रों में गुरु अष्टावक्र का नाम एक दार्शनिक और तत्व चिंतक के रूप में आदर से लिया गया है। वे अष्टावक्र इसीलिए कहे जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर आठ जगह से वक्र अर्थात टेढ़ा था। प्रसिद्ध कथा है – अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे। दोनों ओर ऊंचे आसनों पर सभासद, ज्ञानी, पंडित, राजकर्मी आदि बैठे थे और सामने राजा जनक का सिंहासन था, जिस पर वे विराजित थे। अष्टावक्र उस समय किशोर वय के थे। अष्टावक्र ने जैसे ही जनक की सभा के मुख्य मंडप में प्रवेश किया, उन पर दृष्टि पड़ते ही सभी ने एक-दूसरे की ओर देखा और एक जोरदार ठहाका सभा में गूंज उठा। इस ठहाके की गूंज देर तक सुनाई दी। सभी अष्टावक्र का अजीबो-गरीब व्यक्तित्व देखकर हंस पड़े थे। इतना कि उनकी हंसी रुक न रही थी। यह देख पहले तो अष्टावक्र कुछ समझ न पाए। अष्टावक्र ने जवाब दिया – मुझे लगा मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, जहां व्यक्ति की चमड़ी देखकर उसका निर्णय होता है। जनक सहित पूरी सभा अष्टावक्र के इस उत्तर पर लज्जा से पानी-पानी हो गई। अष्टावक्र ने संदेश दिया कि व्यक्ति का महत्व उसके शरीर से नहीं, उसके ज्ञान, व्यक्तित्व और कर्म से है।
काका हरिओम
भारतीय परंपरा ने क्योंकि नामरूप को अनित्य माना है, इसलिए उसने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इन दोनों की उपयोगिता व्यवहार को लेकर है, शायद इसीलिए उन्होंने इन्हें सिर्फ व्यवहार तक सीमित रखा। देश-काल से परे की सोच रही है यहां के ऋषियों-मनीषियों की।
अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़े थे, ऐसी मान्यता है। पिता ने गर्भस्थ पुत्र को आठ जगह से टेढ़ा होने का शाप दे दिया था। इसीलिए जब वे जन्मे तो आठ स्थानों से टेढ़े थे। अष्टावक्र उनका यह नाम तभी प्रचलित हो गया। कहते हैं न कि विद्या अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती है, बस ऐसा ही कुछ हुआ अष्टावक्र के साथ भी। अष्टावक्र ने भीतर के उस अनुपम सौंदर्य को प्राप्त कर लिया था जिसकी कि छाया मात्र है यह समूचा सांसारिक सौंदर्य।
एक कथा के अनुसार, एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर-उधर से मांग कर थोड़े तंडुल इकट्ठे किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जलाया और मिटटी के टूटे पड़े बरतन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी। लकड़ियां गीली थी इसलिए तंडुल पकने में समय लग रहा था। धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हंंडिया उतारी। उन्हें पत्ते पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। अभी वे एक ग्रास मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया जिसने जनक के उन अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंध गयी। सांस लेना दूभर हो गया। लगा कि प्राण-पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े।
लेकिन यह क्या! सब कुछ बदल गया। नींद खुल गयी। राजभवन को सुकोमल शय्या पर लेटे महाराज जनक का गला रुंधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भीगा हुआ था मानो काफी समय तक होते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया। लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहां थी। एक ही सवाल बेचैन कर रहा था, ‘सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख बिलखता, बेहाल निरीह जनक?’
सुबह उठते हो विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने-अपने उत्तर थे। लेकिन महाराज को कोई संतुष्ट न कर सका। सच क्या है? जागृत अवस्था या कि स्वप्न? यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ गयी।
एक दिन महाराज जनक की विद्वत् परिषद् में जब निस्तब्धता छायी हुई थी, बारह वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। आठ स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गयो। कहीं यह हंसी छिपी थी तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को सम्बोधित किया, “राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वानों-पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं?” वाणी में गाम्भीर्य था और निर्भयता भी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बन ठहर गयी। समूचे वातावरण में एक प्रश्न-सा बिखर गया।
अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया, “मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन्। उठा है, मैं जानता हूं, तो सुनें, चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है। वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिलकुल इसी प्रकार धर्ममयी दृष्टिवाले नाम-रूप को भेदकर उसके भीतर अस्तित्वयान सत्, चित्, आनंद रूप-स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं। राजन् क्या आकाश घट में बंधकर घट-सा हो जाता है, या कि आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकाश बन जाता है?”
सभी अपने-अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। “राजन् मैं यह सुनकर यहां आया था कि आपका कोई प्रश्न है, जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बन कर उसका समाधान चाहते हैं, लेकिन मैंने जो कुछ यहां देखा उससे ऐसा लगा मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन्, यह भी एक व्यसन है।”
बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम् की परतों को मानों उधेड़ दिया था। “मैं आपका आशय नहीं समझा,” महाराज जनक ने निवेदन किया।” आपकी शंकाओं का समाधान कोई तत्त्वजिज्ञासु ही कर सकता है, राजन्! बुद्धि चातुर्य के भोगों में फंसा नहीं जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है, वे नामरूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं। और जो स्वयं नहीं जानता वह किसी की तत्संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है।” महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया।
“तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है?” राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ।” अवश्य राजन! सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना ऐसा है, तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्मतत्व का साक्षाद्नुभव कराऊंगा।” अष्टावक्र के निष्ठापरक वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। ह्रदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो गया। उन्होंने राजसिंहासन से नीचे उतरकर अष्टावक्र के चरणों में दण्डवत् प्रणाम किया। “क्षमा करें। मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर, ज्ञानाम्रत का पान करा अमृतत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म-मरण के चक्र से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा।”
“राजन्, अवश्य होगा! ज्ञान के बिना कोई मार्ग नहीं है। अभेदज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्त्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना राष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्ते हैं राजन्। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पलभर में तुम धन्य हो सकते हो।”
“मुझे क्या करना होगा।” “क्या न्योछावर कर सकते हो?”
“सब कुछ- राज्य, वैभव, परिवार यहां तक कि अपना शरीर भी।” “नहीं, इन सबके कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि छोड़ना चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है, वह नित्य मुक्त है।”
कहते हैं कि इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र काे सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। जब मन ही न रहा तो सहजरूप से संकल्प-विकल्प राग-द्वेष, हानि-लाभ, जीवन-मृत्यु, सुख-दुःख आदि सभी इन्द्र भी तिरोहित हो गए। अन्त:करण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गयी। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्मतत्त्व की अनुभूति हो गयी जितना समय किसी अश्वारोही को एक एड़ से दूसरी एड़ पर रखने में लगता है।
इस प्रकार एक तत्त्वज्ञानी के सान्निध्य में जिज्ञासु राजा जनक ‘विदेह’ बन गए – देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते भी अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त।
‘अष्टावक्र महागीता’ गुरु-शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा उदाहरण है। इसमें गुरु द्वारा दिए तत्त्वज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवाय तत्त्वजिज्ञासु की अनुभूतियों का वह सिलसिला भी है जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुड़-सी अनुभूति है वह।